एक द्रष्टि | Ek Dristi
श्रेणी : साहित्य / Literature
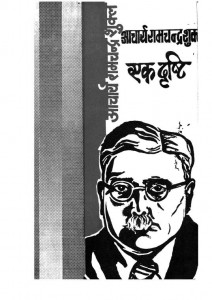
लेखक :
Book Language
हिंदी | Hindi
पुस्तक का साइज :
31 MB
कुल पष्ठ :
247
श्रेणी :
यदि इस पुस्तक की जानकारी में कोई त्रुटि है या फिर आपको इस पुस्तक से सम्बंधित कोई भी सुझाव अथवा शिकायत है तो उसे यहाँ दर्ज कर सकते हैं
लेखक के बारे में अधिक जानकारी :
No Information available about आचार्य रामचंद्र शुक्ल - Aacharya Ramchandra Shukl
पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश
(Click to expand)आचायं रामचन्द्र शुक्ल : एक दृष्टि ११
लगाने में समयें हुए हैं । आचायें शब्द की व्यृत्पत्ति-मुलक अ्थे-हृष्टि* से उनके आचायंत्व का
वह दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण है ।
शुक्ल जी का रस-सिद्धान्त विश्व-समीक्षा सिद्धान्त बनने कीं सम्भावना के प्रतिपादन के
कारण हिन्दी समीक्षा में उसके नवीन महत्त्व का प्रतीक है । शुक्ल जी ने हिन्दी समीक्षा में काव्य के
सभी तत्त्वों का सम्बन्ध रस से नये सिरे से स्थापित किया है । सैद्धान्कि समीक्षा में साहित्य के
विभिन्न सिद्धान्तों की क्या स्थिति होनी चाहिए, किस प्रकार सभी सिद्धान्त अनुभुतिजन्य होने के
कारण रस से सम्बन्धित हो जाते हैं, इसे सर्वप्रथम हिन्दी समीक्षा में बलपुरवेंक आचायें शुक्ल जी
ने ही कहा । हिन्दी समीक्षा में शुक्ल जी के पूर्व रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, औचित्य आदि के
विवेचन बिखरे-बिखरे रहते थे, पूर्वी एवं पश्चिमी समीक्षा के सिद्धान्त अलग-अलग दिखाई पड़ते
थे । इनमें संश्लेघण लाने का कार्य सर्वेप्रथम शुक्ल जी द्वारा रस के माध्यम से संपादित हुआ |
शुक्ल जी ने सर्वेप्रथम रस के दाशंनिक पक्ष से बल, सामाजिक पक्ष पर तथा शास्त्रीय
पक्ष से व्यावहारिक पक्ष पर अवतरित्त किया । उन्होंने अपने रस-विवेचन में रस के मनोवैज्ञानिक
तथा सामाजिक आधार, नैतिक पक्ष, ल्लिकालवरतिनी विश्वात्मक अनुभूति के स्वरूप तथा साधा-
रणीकरण में आलम्बन के लोकधर्मी स्वरूप पर सर्वाधिक बल दिया है । इससे एक ओर तो
उन्होंने रस को लौकिक अनुभूति सिद्ध किया तथा दूसरी ओर अलौकिकता, आध्यात्मिकता को
रस-क्षेत्र से अलग करने का प्रयत्त किया । इन प्रयत्नों के फलस्वरूप वे साहित्य को जीवन के
निकट लाने में तथा उसे सामाजिक बनाने में सर्वाधिक मात्रा में सफल हुए ।
शुक्ल जी के अंग-सिद्धान्तों का विवेचन भी उनके अंगी-सिद्धान्त -- रस-सिद्धान्त के समान
ही प्राचीन भारतीय काव्यशास्त्र का आधार लेने पर भी नवीनता रखता है। अलंकार-विवेचन
में कल्पना का प्रयोग, उसके प्रयोग के मनोवैज्ञानिक कारणों का विचार, रूप; गुण, क्रिया तथा
प्रभाव के आधार पर उसका वर्गीकरण, जीवन-सौन्दर्य के पर्याय-रूप में उसकी स्वीकृति शुक्ल जी
सर्वप्रथम भारतीय समीक्षा में की । वे काव्य में अलंकार को वर्णेत-प्रणाली मानकर उसका स्थान
अन्य अंग तत्त्वों के समान रूप में ही स्वीकार करते हैं । अलंकार-सम्बन्धी उनका उपर्युक्त मत
हिन्दी के परवर्ती समीक्षकों में निविवाद रूप से मान्य हो गया है । हिन्दी के अलंकार-ग्रन्ों में
संस्कृत अलंकार-ग्रन्यों की देखा-देखी स्वभावोक्ति, उदात्त, अत्युक्ति, हेतु आदि _वष्यं से
संबंध रखने वाले अलंकार अलंकारों की श्रेणी में रखे जाते थे । इनका सम्बन्ध वष्यें से होने के
कारण शुक्ल जी ने इनके अलंकारत्व का निषेध किया है । यह घारणा उनके परवर्ती समोक्ष कों
को भी मान्य-सी हो गई है । अलंकारों की संख्या के विपय में शुक्ल जी का. विचार बहुत ही
प्रगतिशील ढंग का है, क्योंकि वे उनकी इयत्ता नहीं मानते । उनकी दृष्टि में नये अलंकारों के
आविष्कार की सम्भावना प्रत्येक कवि तथा कृति में है । इस प्रकार शुक्ल जी की प्रगतिशील
मलंकार-घारणा हिन्दी के अलंकार-सम्बन्धी मत को उसकी संकुचित यंत्रगतिक श्छूंखला से उन्मुक्त
कर उसे विस्तृत रूप देती है ।
शुक्ल जी की रीति-सम्बन्धी व्याख्या आज हिन्दी-समीक्षकों के बीच रीति-सम्बच्घी मान्य
घारणा के रूप में प्रचलित है । रीतिवादियों के समान आज हिन्दी का कोई समीक्षक रीति को
काव्यात्मा नहीं मानता । शुक्ल जी ने रीति का सम्बन्ध भाषा से, पद-संघटना से, शेली से मानते
हुए उसका सम्बन्ध काव्य के बहिरंम-पक्ष से स्थापित किया है । रीति के सम्बन्ध में यही धारणा
हिन्दी-समीक्षा में आज भी प्रचलित है ।


User Reviews
No Reviews | Add Yours...