सिरिवालचरिउ | Sirivalchariu
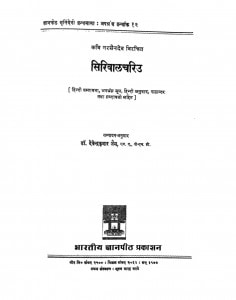
लेखक :
Book Language
हिंदी | Hindi
पुस्तक का साइज :
39 MB
कुल पष्ठ :
176
श्रेणी :
हमें इस पुस्तक की श्रेणी ज्ञात नहीं है |आप कमेन्ट में श्रेणी सुझा सकते हैं |
यदि इस पुस्तक की जानकारी में कोई त्रुटि है या फिर आपको इस पुस्तक से सम्बंधित कोई भी सुझाव अथवा शिकायत है तो उसे यहाँ दर्ज कर सकते हैं
लेखक के बारे में अधिक जानकारी :
No Information available about देवेन्द्र कुमार जैन - Devendra Kumar Jain
पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश
(Click to expand)दो शब्द
कश्यकी सम्परेपणीयताकी दृष्टि से “सिरिवा चरिउ बेजोड कान्य है 1 श्रीपाल जैसे पुराण काव्यके
नायक को दो सन्धियोंके लूघु काव्यमें इस प्रकार चित्रित कर देना किं पौराणिक गरिमा ओर मानवी संवेदना
एक साथ बनी रहे, यह् कवि नरमेन के ही बृतेका काम था !
लम्बे अरसेसे सोच रहा था कि किसी 'अपभरंश-चरित-काव्य' का सम्पादन कं । मुख्य कठिनाई थी,
किसी उपयुक्त और महत्त्वपूर्ण पाण्डुलिपिकी प्राप्तिकी । इसे हल करनेका श्रेय है, डॉ. कस्तुरचन्द्र कासरीवाल
जयप्रको । उन्होंने एक नहीं--तीन-तीन प्रतियाँ महावीर भवन जयपुरसे भिजवानेकी व्यवस्था की ।
जिस समय मैं सम्पादन कर रहा था, अचानक एक साथ कई आपत्तियाँ आयीं और सारा काम
अस्तव्यस्त हो गया । परिस्थितियोंसे जूझनेके बाद जो समय बचता, मैं उसमें सम्पादन करता रहता, यह
सोचकर कि यदि श्रीपार लकड़ीके दुकड़ेके सहारे समुद्र तिर सकते हैं तो कया मैं इस काममें लगे रहकर
धाओंसे उत्पन्न मानसिक ततावकों कम नहीं कर सकता ? आपत्तियाँ गिनानेसे लाभ नहीं क्योकि पाठकोको
पालके जीवनमें ही संसारका इतना उतार-चढ़ाव मिलरू जायेगा कि कहीं उनका मन संवेदनासे सक्रिय हो
उठेगा और कहीं वे भाग्यकी विडम्बनाकों कोसेंगे, कहीं करुणासे उत्को आँखें नम हो उठेंगी और कहीं
धवलसेठके काले कारनामे उनके हुदयको सफेद बनायेंगे । श्रीपाल और घवलसेठ जीवनके दो पक्ष हैं--एक
सत् प्रवृत्तिका प्रतीक है और दूसरा असत् का ।
'सिरिवाल् चरिडउ की पाण्डुलिपियाँ सोलहवीं सदीके दूसरे और तीसरे चरणके बीचकी उपलब्ध हैं ।
यह वहू समय हैं, जंब आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओंका न केवछ विकास हो चुका था, बल्कि उसमें साहित्यकी
रचना भी होने छगी थी । इन नयी-नयी भाषाओंमें जैन साहित्य भी मिलता है । परन्तु इस समय, अपभंश-
चरित काव्यकी धारा भी चली रही थी) अतः परवर्ती भाषाओंके विकासके विचारसे इस प्रकारकी
1हित्य कृतियोंका बया महत्त्व और सीमाएँ होनी चाहिए ? यह एक विचारणीय प्रश्न है । कतिपय जैन छेखक
१८वीं सदी तक अपभ्रंशकी 'चरित दौछी को एक काव्यरूढ़िके रूपमें अपनाये रहे । युग और नयी भाषाओंके
बसे आलोच्य काव्यकी भाषामें मिलावट न होता आइचर्यकी बात होती । इसमें दो मत नहीं कि इसकी भाषा
तथाकथित परिनिष्ठित अपभ्रंश तहीं है; परन्तु उसमें उतनी अव्यवस्था और अप्रामाणिकता भी नहीं है जो
हमें पृथ्वीराज रासोकी भाषामें दिखाई देती है । पण्डित तरसेन द्वारा लिखित पाण्डुकिपि न मिलनेसे भी
ठोंका निश्चय और अर्थ करने में बहुत कठिनाई हुई है । प्रतिलिपिकारोंने हस्व-दीर्घ, शब्दस्वरूप, अनुस्वार
तासिकध्वनि यू व् श्रुतिके प्रयोगमे मनमानी की ह । सम्पादनके लिए मुझे पहले दो प्रतियाँ मिलीं । उनके
आधारपर॑ मैंने पूरी रचनाका सम्पादित पाठ तैयार कर लिया। बादमें ज्ञानपीठके विद्वान् सम्पादकोंने सुझाव
दिया कि एक और प्रतिका उपयोग करना जरूरी है। फलस्वरूप तीसरी प्रति उपलछब्ध कर दुबारा सम्पादित
पाठ प्रस्तुत किया । फिर भी उसमें भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा निर्धारित आदर्शपाठकी दृष्टिसे कुछ कमियाँ रह
गयीं । फछतः तीसरी बार पुनः पूरी प्रतिको संवारता पड़ा । यह सब हो चुकनेके बाद, जो प्रश्न मुझे खटकता
रहा वह यह कि 'सोलहूवीं सदी के अपभ्रंशचरित॒काव्यकी भाषा और पाठोंमें जो मिलावट या नयापन है,
उसके आरेमें क्या किया जाये | संक्रमणयुगके एेसे प्रन्थोके सम्पादलके किए वही नियम ओर प्रतिमान उपयोगी
नहीं हो सकते जो १०वीं सदीके अपभ्रंशचरित कांब्योंके सम्पादनके लिए मान्य किये जा चुके हैँ और जिनके
आधारपर विविध अपभ्रंशचरितकाव्य सम्पादित हुए हैं, सम्भवतः यह समस्या ज्ञानपीठके सम्पादकोके मनमं
र श्रद्धेय डॉ. हीराछाल जीने न केवल पूरे मूलपाठका संशोधन किया बल्कि कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव
इनमेंसे कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं ।


User Reviews
No Reviews | Add Yours...